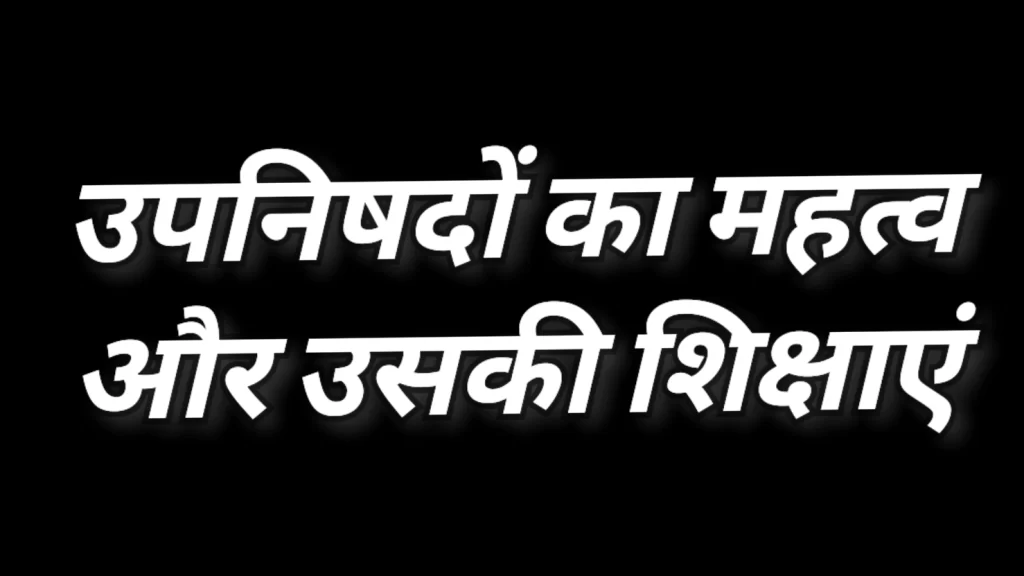उपनिषद ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ हैं। प्रामाणिक 12 उपनिषदों में ब्रह्मविद्या का दार्शनिक स्तर पर विवेचन किया गया है। उपनिषदों में समाज के परिष्कार को ध्यान में रखकर आत्म-परिष्कार की चर्चा की गई। उपनिषदोंं के अनुशीलन से इस निष्कर्ष पर पहुँचना सरल है कि उपनिषद ग्रन्थ निष्काम कर्मयोग के आधार पर सामाजिक कार्यों की शिक्षा प्रदान करते रहे हैं।
उपनिषदों का ज्ञान ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया का फल प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुरोहित जब यज्ञादि कर्मकाण्ड पर अधिक बल देने लगे तो उसकी प्रतिक्रिया में उपनिषदों की रचना हुई। जब यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले पुण्य फलों का अवसान होने लगा तब चिंतन-मनन के द्वारा ऋषियों और विद्वानों ने ब्रह्मज्ञान या तत्वज्ञान का अन्वेषण किया। इस अन्वेषण के आधार पर यह स्थापित किया गया कि ज्ञान मार्ग पर चलने से मनुष्य के सब दुखों का निवारण इसी लोक में सम्भव है।
यहाँ उपनिषदों के महत्व और उनकी शिक्षाओं का अवलोकन किया गया है।
कर्मपरायणता
वेदों के कर्मवाद को उपनिषदों में निष्काम कर्मयोग का स्वरूप प्रदान किया गया है। उपनिषदों ने समाज को आशावादी बनाने के लिए सौ वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित रहने की शिक्षा दी। त्याग की नीति को अपनाकर कर्मरत रहने की शिक्षा उपनिषदों में दी गई है। कर्मपरायण मार्ग को निश्चित करते समय समस्त सदाचार को सम्यक् मान्यता दी गई। किसी अन्य के धन को मृत्तिका समझने का उपदेश दिया गया है।
नित्य नैमित्तिक कर्मों को करने के साथ-साथ उपासना से सम्बद्ध कर्मों को करने की भी प्रेरणाएं दी गयी हैं। अशुभ मार्ग पर चलना आत्मा का हनन करना है अतः ईमानदारी से ही कार्य करना चाहिए।
‘बृहदारण्यकोपनिषद्’ में महर्षि याज्ञवलक्य के प्रसंग में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गृहस्थ को सुचारु रूप से संचालित करके ही परमार्थ की साधना हेतु प्रयाण करना चाहिए। अग्निहोत्र सम्पादित करते हुए वातावरण को पवित्र बनाना चाहिए। सत्य एवं मृदुवचन बोलकर वाणी का तप करना चाहिए। जो कार्य प्रशंसनीय हैं, उन्हीं को करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक कर्मठता को अपनाना चाहिए। जिन आदर्शों को अपनाने से चरित्रवान बन सकते हैं, उन्हें अवश्य ही अपनाना चाहिए। कर्मपरायणता आत्म-ज्ञान की प्राप्ति में नितान्त सहायक तत्त्व है।
निरहंकारता
‘केनोपनिषद्’ में अहंकारी भावना को स्पष्ट किया गया है। एक ज्ञानी व्यक्ति वह है जो यथार्थ को जानकर भी यही कहता है कि मैंने यथार्थ को नहीं जाना। जो व्यक्ति कुछ ग्रन्थों का अध्ययन करके यथार्थ तत्व को जानने का दावा करता है, उसने यथार्थ को नहीं जाना।
‘छान्दोग्योपनिषद्’ में रैक्व ऋषि के आख्यान द्वारा निरहंकारता की शिक्षा दी गई है। नारद-सनत्कुमार संवाद के माध्यम से भी निरहंकारता के महत्व को स्थापित किया गया है। इसी प्रकार ‘ईशावास्योपनिषद’ में अज्ञानी पुरुष के अहंकार की आलोचना की गई है। उपनिषदों में कहा गया है कि अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति पतनोन्मुख होता है। अतएव निरहंकारता परम आवश्यक गुण है। अहंकार के त्याग का एकमात्र आधार आध्यात्म विद्या ही है।
मुमुक्षा
मुमुक्षा का अर्थ है मोक्ष की कामना। उपनिषद ब्रह्मविद्या के प्रस्तुतकर्त्ता ग्रन्थ होने के कारण पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष को सर्वाधिक महत्त्व देते रहे हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शामिल हैं। मोक्ष को जीवन की अंतिम एवं श्रेष्ठ परिणति माना गया है। मोक्ष जीवन का परमार्थिक लक्ष्य है।
नित्य नैमित्तिक कर्मों को सम्पादित करने के क्रम में मोक्ष प्राप्ति की सबल इच्छा रहनी चाहिए। एक मुमुक्ष व्यक्ति समस्त सांसारिक सिद्धियों या सफलताओं को प्राप्त करते हुए भी अपने आत्मरूप को प्राप्त करने के लिए सचेत रहता है। मुमुक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह एकान्त परायण बने।
‘बृहदारण्यकोपनिषद्’ में मोक्ष की महत्ता को स्थापित किया गया है। मोक्ष की इच्छा के कारण निष्काम कर्मयोग साकार होता है। निष्काम कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति अनन्त ज्ञान के पथ पर अग्रसर होता है। जहाँ मुमुक्षा है, शान्ति वहीं है।
आत्मज्ञान
उपनिषदों में आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। गूढ़ तत्व आत्मा का सबके सामने प्रकाश नहीं होता। आत्मा केवल सूक्ष्म दृष्टि से अथवा ज्ञान-नेत्रों से ही दर्शनीय है। आत्मा का निवास हृदय के रोहिताकाश नामक भाग में कहा गया है। आत्मज्ञानोन्मुख व्यक्ति जरा- मरण के चक्र से निवृत्त हो जाता है।
श्वेताश्वरोपनिषद् में योगसाधना को आत्मज्ञान का मूल कारण सिद्ध किया गया है। एक साधक एकान्तसेवी होकर, भय को त्याग कर, स्वस्थ मन से निरन्तर आत्म-चिन्तन करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति के चित्त में सहज सुख की अनुभूति होती रहती है।
‘कठोपनिषद्’ में कहा गया है कि शरीर रूपी रथ में आत्मा रूपी रथी बैठा हुआ है। बुद्धि रूपी सारथी इन्द्रिय रूपी घोड़ों की मन रूपी रस्सी को पकड़कर शरीर रथ को संचालित करता है। जिस व्यक्ति की इन्द्रियां असंयमित हैं, अथवा जिनकी बुद्धि अस्थिर है, उस व्यक्ति का अधःपतन अवश्यम्भावी है।
जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति तथा तुरीय नामक चार अवस्थाओं के क्रम में व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान पुरुषार्थलभ्य होता है। कोई बलहीन व्यक्ति, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मज्ञान प्रवचन से भी प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति शास्त्र विधि के द्वारा आत्मा की ओर बढ़ता है, आत्मा का प्रकाश उसके सामने स्वतः प्रकट हो जाता है तथा वह व्यक्ति आत्मरूपता को प्राप्त कर लेता है।
संसार की असारता
उपनिषदों में संसार की शिक्षा अनेक रूपों में दी गई है। जब एक व्यक्ति अन्न को अपने जीवन का सर्वस्व मानता है, तो उसे अपनी आत्मा अन्न के रूप में जान पड़ती है – अन्नमेव प्राण। जब व्यक्ति ‘उपाहम्’ से थोड़ा ऊपर उठता है तो उसे प्राणशक्ति का अनुभव होता है और वह प्राणशक्ति को ही अपनी आत्मा मानने लगता है।
जब वही व्यक्ति मन के स्वरूप को समझता है तो उसे मन ही आत्मा के रूप में जान पड़ता है। वही व्यक्ति बुद्धि-तत्व का महत्त्व समझ कर बुद्धि या विज्ञान-तत्व को अपनी आत्मा मानने लगता है। ऐसा विज्ञानवादी व्यक्ति विशुद्ध आनन्द का अनुभव करके आनन्द-तत्व को ही आत्मा मानने लगता है। आनन्द का आत्म-तत्त्व के रूप में अनुभव करने पर समस्त संसार फीका लगने लगता है। व्यक्ति शिव-तत्व को जानकर संसार की असारता को भली-भांति समझ जाता है।
ईश्वरीय ज्ञान
सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म अर्थात् सत्य एवं अनन्तश ज्ञानस्वरूप ईश्वर को जानना ही अनन्त ज्ञान को प्राप्त करना है। ईश्वरीय ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करके ईश्वर रूप ही हो जाता है–ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति।
जब एक व्यक्ति की समस्त वासनाएँ छिन्न-भिन्न हो जाती हैं तब वह अमरता का वरण करता है। जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में मिलकर विश्राम करती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा ईश्वर में विलीन होकर अखण्ड आनन्द को प्राप्त करती है। ईश्वरीय ज्ञान आत्मा का ही ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान होने पर सम्पूर्ण जगत् ईश्वरवत् प्रतीत होने लगता है – सर्वम् खल्विद ब्रह्म।
उपनिषदों में सत्य और यथार्थ ज्ञान के रूप में ईश्वरीय ज्ञान को ही स्वीकार किया गया है। इसी से मुक्ति या मोक्ष सम्भव है।
पुनर्जन्म
छान्दोग्य उपनिषद में कहा गया है कि अल्प धार्मिकता या साधना में सुख नहीं है। सुख की असीमता केवल अखण्ड साधना शक्ति में ही होती है। जब तक जीव कर्मों के बन्धन में बंधकर भटकता है तब तक उसे जन्म-जन्मान्तर के रूप में विभिन्न योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। जीव आत्मरूपता को प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म के चक्र से दूर हट जाता है।
‘श्वेताश्वतरोपनिषद्’ में कहा गया है कि योगानल-सदृश शरीर को पाने वाले योगी को जरा-मरण के बन्धन से मुक्ति मिल जाती है।
स्वाध्याय की महिमा
सद्ग्रन्थों के नियमित अध्ययन को स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय से व्यक्ति के मानस में निहित भावनाओं को जागृति का अवसर मिलता है। उपनिषद ग्रन्थों का स्वाध्याय करने से नित्य पावन पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है।
स्वाध्याय की महिमा को कठोपनिषद् में यम और नचिकेता के प्रसंग में स्पष्ट किया गया है। उपनिषदों में स्वाध्याय की महिमा का प्रकाशक ग्रन्थ ‘तैत्तिरीयोपनिषद्’ है। मुण्डकोपनिषद् में भी स्वाध्याय के रहस्य पर प्रकाश डाला गया है। ‘छान्दोग्य’ तथा ‘बृहदारण्यकोपनिषद्’ में विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से स्वाध्याय की महिमा उल्लेख किया गया है।
अतः उपनिषदों में यथार्थ ज्ञान के मार्ग पर चलने का एकमात्र आधार स्वाध्याय को ही सिद्ध किया गया है।
गुरु का महत्व
वेदविद् गुरु के महत्व के प्रकाशन के लिए कठोपनिषद् में अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई हैं। ज्ञान-पिपासु शिष्य को वेदज्ञ गुरु को खोजना चाहिए क्योंकि उसके अभाव में ज्ञानसूर्य से आलोकित पथ पर चलना असम्भव है।
जो गुरु यथार्थ ज्ञान को पाकर प्रायः मौन साधे रहता है अथवा गम्भीर बना रहता है, वही ययार्थ गुरु होता है। समस्त औपनिषदिक ज्ञान गुरुजनों की ही देन हैं। उपनिषदों में ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु कहा गया है। गुरुजनों के ज्ञानलोक से संसार अज्ञान-अन्धकार को दूर करता है तथा सामाजिक व्यवस्थाएं सुचारु रूप से सम्पन्न हुआ करती हैं।
कठोपनिषद् के ‘अज्ञानेनैव नीयमाना यथान्धा’ रहस्य को महात्मा कबीर ने निम्न रूप में प्रस्तुत किया है –
जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरध।
अन्धा अन्धेहिं ठेलिया, दोनों कूप परन्त॥
शिष्य का कर्तव्य
उपनिषदों में विद्यार्थियों के कर्तव्यों का व्यापक उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी को चाहिए कि वह माता-पिता को देवतुल्य समझे। विद्यार्थी का यह कृत्य है कि वह यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु को ढूंढे।
‘कठोपनिषद्’ में नचिकेता ने आचार्य यम को ढूंढकर आध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया, यह स्पष्टतः बताया गया है। इसी प्रकार ‘प्रश्नोपनिषद्’ में अनेक आचार्यों तथा शिष्यों के प्रश्नोत्तरों की चर्चा भी यही सिद्ध करती है कि विद्यार्थी को ज्ञानवर्धन के लिए विद्वान् गुरुजनों की खोज करनी चाहिए।
विद्यार्थी तर्क और सेवा के द्वारा सदैव ज्ञानार्जन करे, यह उपनिषदों की शिक्षा है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। उपनिषदों में ब्रह्मचर्य और विद्यार्जन का अटूट सम्बन्ध स्थापित किया गया है। विद्यार्थी के लिए एकान्तवास तथा दत्तचित्तता को अनिवार्य बताया गया है।
वस्तुतः उपनिषदों से जीवन को एक अपूर्व प्रेरणा मिलती है। उनके मन्त्र प्रगतिशील और जागरूक हैं। उपनिषद साधारण जन तक को बराबर सतर्क करती रहती है –
उत्तिष्ठत जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत।
अर्थात् ‘उठो, जागो और बड़ों के पास जाकर सीखो – ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि अमर हो जाओ।
उपनिषद से जुड़ी जानकारी के लिए आप इन आलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं –
उपनिषदों के नाम एवं उनका संक्षिप्त परिचय
उपनिषद क्या हैं?
उपनिषदों का विवेच्य विषय