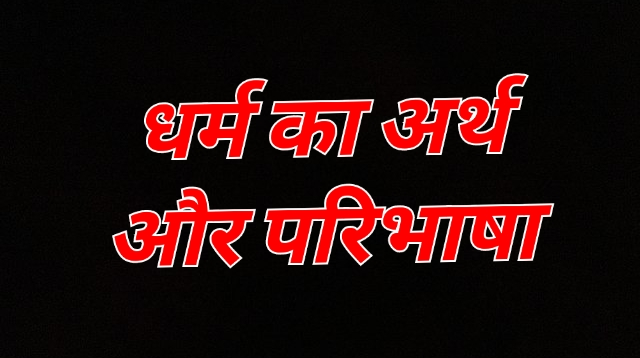धर्म शब्द संस्कृत का एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ बड़े व्यापक होते हैं। इस शब्द का अनुवाद संसार की किसी भी भाषा के एक शब्द में नहीं किया जा सकता। धर्म शब्द का पर्याय है पुण्य, श्रेय, सुकृत, वृष (सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला), न्याय, स्वभाव, आचार, उपमा, ऋतु, अहिंसा, उपनिषद्, धनु, यम, सोमप, सत्संग इत्यादि।
धर्म का स्वरूप इतना विशाल है कि उसको किसी एक व्याख्या में नहीं बांधा जा सकता है। इस प्रकार अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार विभिन्न विचारकों ने धर्म की अनेक व्याख्याएँ की हैं।
‘धर्म’ शब्द की व्युत्पत्ति
‘धर्म’ शब्द की व्युत्पत्ति विभिन्न प्रकार से की गई है।
धर्म शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता आया है। शब्दकोश में इसके लिए विविध शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे – नियम, कर्तव्य, अधिकार, न्याय, नैतिकता, गुण इत्यादि।
अनन्त अपौरुषेय वेद ने धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा कहकर धर्म को जगत की प्रतिष्ठा बताया है। जगत् में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जिसमें धर्म विद्यमान न हो; ऐसा कोई तत्त्व नहीं, जिसमें धर्म की सत्ता न हो।
‘धर्म’ शब्द ‘धृ’ धातु से बना है। धृ धातु धारण, पोषण और अवस्थान आदि दस अर्थों में प्रयुक्त होता है। धारण करने के अर्थ में कहा जाता है जो तत्व सारे संसार के जीवन को धारण करता हो, जिसके बिना लोक-स्थिति सम्भव न हो, जिससे सब कुछ संयमित, सुव्यवस्थित एवं सुसंचालित रहे, वह धर्म है।
संसार धर्म पर ही टिका हुआ है। यदि संसार में सब अपना-अपना धर्म छोड़ दें तो विश्व एक दिन भी नहीं टिक सकता। पृथ्वी का धर्म है धारण करना, वायु का धर्म है हवा चलाना और पानी का है प्यास बुझाना। यदि ये सब अपना-अपना धर्म छोड़ दें तो क्या क्षणभर भी जगत् टिक सकता है? इसी प्रकार मानव मानव का धर्म, पिता पिता का धर्म, माँ माँ का धर्म, स्त्री स्त्री का धर्म छोड़ दे तो जगत् नहीं चल सकता।
धर्म का शब्दार्थ होता है, धारणाद् धर्मः अर्थात धारण करना, दुःख से बचाना। इस रूप में धर्म वह है, जो हमें सब तरह के विनाश और अधोगति से बचाकर उन्नति की ओर ले जाता है।
किसी वस्तु के जो गुण ऐसे हैं जिनसे वह अपने रूप में धारित रहती है, बनी रहती है, उन गुणों को उस वस्तु का धर्म कहा जाता है। इस यौगिक अर्थ के आधार पर प्रयोग में धर्म शब्द के बड़े विस्तृत अर्थ हो जाते हैं। किसी वस्तु के भौतिक और रासायनिक गुण उसके धर्म हैं। किसी वर्ण और आश्रम के नियम और कर्तव्य उसके धर्म हैं। राज्य नियम धर्म हैं।
इसीलिये कानून की पुस्तकों को संस्कृत में धर्मशास्त्र कहा जाता है। राज्य नियमों के अनुसार न्याय करने को धर्म कहा जाता है। न्यायाधीश को धर्माध्यक्ष और धर्माधिकारी कहा जाता है और न्यायालय को धर्माधिकरण कहा जाता है। इसी भांति किसी सभा समाज के नियमोपनियम उसके धर्म हैं। आत्मा. परमात्मा, परलोक और कर्मफल में विश्वास और इस विश्वास के आधार पर परमात्मा की उपासना और तदनुकूल आचरण को भी धर्म कहते हैं।
धर्म का एक अन्य अर्थ है – धिन्वनाद् धर्मः।
धिन्वन का अर्थ है धारणा या आश्वासन देना, दुख से पीड़ित समाज को धीरज देकर सुख का मार्ग दिखाना। इस प्रकार के आचार का नाम धर्म है।
व्याकरण की रीति से धारणार्थक ‘धृञ्’ धातु से ‘मन्’ प्रत्यय करने पर धर्म शब्द की सिद्धि होती है। उसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है।
ध्रियते लोकः अनेन – जिसके द्वारा लोक धारण किया जाय उसे धर्म कहते हैं।
धारयति लोकम् – जो लोक को धारण करे, उसे धर्म कहते हैं।
धर्म शब्द की परिभाषा इस प्रकार है –
ध्रियत इति धर्मः, धार्यत इति धर्मः, पतितं पतन्तं पतिप्यन्तं धरतीति धर्मः।
सारा कार्य-व्यापार जिसके द्वारा धारित होता है, जो कार्य-कारण का आश्रयस्वरूप है, जो अपने में गिरे हुए, गिरते हुए और गिरने वाले मनुष्यों को अवनति के मार्ग से बचाकर उन्नति की ओर ले जाने की शक्ति धारण करता है; वही धर्म कहलाता है।
जो व्यक्ति से लेकर समाज तक की व्यवस्था रखने का सुखमय मार्ग दिखाने का सामर्थ्य रखता हो, जिसमें व्यक्ति, समाज; तथा राष्ट्र के कल्याण के लिये नियम, नीति, न्याय, सत्य, सद्गुण, सदाचार, सुस्वभाव, स्वार्थत्याग, कर्तव्य-कर्म और ईश्वरभक्ति आदि उत्तम गुण विद्यमान हों तथा जो लौकिक और अलौकिक श्रेय का साधन हो, वही वास्तविक धर्म कहलाता है, वही परिपूर्ण धर्म है।
धर्म के भेद
स्मृति ग्रन्थों में धर्म के भेदों का विशद वर्णन मिलता है। स्थूल दृष्टि से धर्म के तीन भेद होते हैं।
- साधारण धर्म, 2. विशेष धर्म, 3. आपद्धर्म
ये तीनों धर्म मनुष्यमात्र के लिये कल्याणकारक होते हैं।
सामान्य धर्म
सामान्य धर्म सर्वलोकोपकारी, शास्त्रसम्मत, सबके लिये यथायोग्य अधिकारानुसार आचरणीय और सर्वथा वैध होता है।
सत्य, दया, दान, मन- संयम, इन्द्रियों का दमन, सहनशीलता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, नम्रता, स्वाध्याय, संतोष, सेवा, समदृष्टि, विषय- भोगो में आसक्ति का अभाव, हित-मित-सत्य भाषण, परिमित व्यवहार, भगवान् के पुण्य चरित्रों का श्रवण, सत्पुरुष का संग, बुद्धि की स्थिरता आदि सामान्य धर्म हैं।
किसी भी जाति, किसी भी देश या किसी भी काल का रहने वाला क्यों न हो, सबके लिये जरूरी हैं ये। चाहे कोई संन्यासी हो या वैरागी, अद्वैतवादी हो या विशिष्टा- द्वैतवादी, भक्त हो या ज्ञानी, रसिक हो या अरसिक – ये नियम, ये धर्म सबके लिये बराबर पालनीय हैं।
सनातन धर्म प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की अनुमति देता है कि सब अपने-अपने क्षेत्र में रह कर सामान्य धर्म तथा यम, नियम और संयम का जीवन व्यतीत करें। अर्थात् जितना जिससे बन पड़े उतना पालन करें। सनातन धर्म किसी पर कोई दबाव नहीं डालता।
शास्त्र- विरुद्ध आचरण किसी भी समय किसी भी हेतु से किसी के भी लिये नहीं करना चाहिये। यही सर्वसाधारण के लिये पालनीय सनातन धर्म है। परंतु जो मनुष्य जिस विषय में जैसा व्यवहार करता हो, उससे वैसा व्यवहार करना धर्म है। कपटी को कपट व्यवहारों से बाधित करना चाहिये और साधु आचरण वाले के साथ वैसा सदाचरण करना चाहिये। तात्पर्य यह कि यदि कोई लाठी से प्रहार करता हो तो उसे लाठी से रोकना सामान्य धर्म में उचित ही है।
विशेष धर्म
धर्म सार्वभौम है, सबके लिये है तो उसका समयानुकूल तथा साधक की परिस्थिति तथा अधिकार के अनुरूप भिन्न-भिन्न रूप भी होगा। इसलिये प्रत्येक युग के विशेष-विशेष धर्म हैं। प्रत्येक वर्ण एवं आश्रम के भिन्न-भिन्न धर्म हैं। प्रत्येक के अधिकार के अनुसार भिन्न-भिन्न धर्म हैं। विशेष धर्म मनुष्य को कठिनाई सहन करना और तपोमय जीवन व्यतीत करना सिखाता है।
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते।
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे॥
अर्थात् सतयुग में तप की, त्रेता में ज्ञान की, द्वापर में यज्ञ की और कलियुग में दान-धर्म की प्रधानता होती है। इसी प्रकार कलियुग में स्वल्पानुष्ठान से ही विशेष धर्म की प्राप्ति कही गयी है।
विशेष धर्म में आते हैं— वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म इत्यादि। इनमें जिसके लिये जो विहित है, उसी के लिये वह धर्म है।
विशेष धर्म जिसके लिये विहित है, उसी को उसका अनुष्ठान करना चाहिये। इसी विशेष धर्म को लेकर भगवान ने गीता में कहा है-
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥
विशेष धर्म में निज स्वार्थ का त्याग तो होता ही है, प्रिय-से-प्रिय सम्बन्धियों, वस्तुओं और परिस्थितियों का त्याग भी सुखपूर्वक कर दिया जाता है। एक परम धर्म के लिये सभी छोटे-छोटे धर्मों का त्याग हो जाता है। इसी प्रकार आत्मीय स्वजनों का त्याग भी होता है।
पिता तज्यौ प्रहलाद, बिभीषन बंधु, भरत महतारी।
बलि गुरु तज्यौ कंत ब्रज बनितनि, भये जग मंगलकारी॥
भगवान् से द्रोह रखने वाले पिता की बात प्रह्लाद ने नहीं मानी, विभीषण ने बड़े भाई रावण का त्याग कर दिया। भरत ने रामविरोधिनी माता से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया, बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात न मानकर वामन भगवान् को दान किया और ब्रजांगनाओं ने अपने-अपने पतियों को छोड़ दिया। पर ये कोई भी पापी नहीं हुए, न परिणाम में इन्होंने दुख ही भोगा, वरन् सारे संसार के लिये इनका चरित्र कल्याणकारी हो गया।
विशेष धर्म भी दो प्रकार का है – नारी धर्म और पुरुष धर्म । गृहस्थ आश्रम में पुरुष धर्म और नारी धर्म का समुचित समन्वय होता है। गृह का अर्थ घर नहीं प्रत्युत स्त्री है। जब किसी पुरुष का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार किसी स्त्री से सम्बन्ध स्थापित होता है तभी वह गृहस्थ कहलाता है। पुरुष धर्म और नारी धर्म की सफलता पर ही गृहस्थाश्रम की सफलता निर्भर है।
पुरुष धर्म के भी दो भेद हैं – वर्ण धर्म और आश्रम धर्म। वर्ण धर्म के अनुसार धर्मानुष्ठान करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। जो जिस वर्ण का है उसको उसी वर्ण-धर्म का पालन करना चाहिए। हिन्दू जाति की बुनियाद वर्ण धर्म पर आश्रित है।
आपद्धर्म
मनुष्य सदा सामान्य परिस्थिति में नहीं रहता। रोग, शोक, विपत्ति आदि आती ही रहती हैं। शास्त्र में ऐसी परिस्थिति में धर्म के निर्वाह के लिए विधान किया गया है। उस परिस्थिति में सामान्य अथवा विशेष धर्म में कुछ छूट दी गयी है; किंतु उतनी ही छूट दी गई है जिससे जीवन निर्वाह संभव हो सके।
एक बार अकाल पड़ा। एक ऋषि भूख से मरणासन्न थे। प्राण रक्षा के लिये उन्होंने शूद्र से उसके उच्छिष्ट उबाले उड़द लिये। शूद्र ने जल देना चाहा तो ऋषि ने कहा– ‘तुम्हारा उच्छिष्ट जल लेने से मैं धर्मभ्रष्ट हो जाऊँगा। जल मुझे अन्यत्र भी मिल सकता है। प्राण रक्षा के लिये मैंने उड़द लिये ताकि प्राण रखकर धर्म पालन तथा आराधना कर सकें।’
यह दृष्टान्त आपद्धर्म की मर्यादा को बहुत स्पष्ट करता है। किंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि आपद्धर्म धर्म नहीं है। अत्यन्त विवशता में केवल प्राणरक्षा के लिये धर्म में किंचित् शिथिलता की वह छूट है।
धर्म के प्रकार
मेधातिथि, हेमाद्रि व्रत खण्ड में उद्धृत तथा भविष्यपुराण के अनुसार धर्म के पाँच प्रकार हैं – वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गौण धर्म और नैमित्तिक धर्म।
- वर्ण धर्म – एक वर्ण का आश्रय लेकर जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसको वर्ण धर्म कहते हैं—जैसे उपनयन आदि।
- आश्रम धर्म – आश्रम को आश्रय करके जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसको आश्रम धर्म कहते हैं—यथा भिक्षा तथा दण्डादि धारण ।
- वर्णाश्रम धर्म – वर्णत्व और आश्रमत्व को अधिकार करके जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं जैसे मेखलादि धारण।
- गुण धर्म – जो धर्म गुण के द्वारा प्रवर्तित होता है, उसे गुण धर्म कहते हैं— जैसे नियमपूर्वक प्रजापालन आदि।
- नैमित्तिक धर्म – किसी निमित्च को आश्रय करके जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं—जैसे प्रायश्चित्त विधि आदि।
इन पांचों स्वरूपों में मानव जीवन धर्म से ओतप्रोत हो सकता है; क्योंकि ये उक्त स्वरूप जीवनशृंखला में परस्पर अनुस्यूत हैं।
वहीं गुण-भेद के अनुसार धर्म तीन प्रकार के हैं- सात्विक धर्म, राजस धर्म और तामस धर्म।
- सात्विक धर्म – जिन कर्मों में किसी प्रकार की फल-कामना नहीं होती। ये ही कर्म हमारे कर्तव्य कर्म है, इस प्रकार की बुद्धि से जो कर्म अनुष्ठित होते हैं उनको सात्विक धर्म कहते हैं।
- राजस धर्म – मोक्ष के निमित्त संकल्प करके जो कार्य अनुष्ठित होते है, उनको राजस या राजधर्म कहते हैं।
- तामस धर्म – कर्म में विधि की अपेक्षा न करके केवल कर्मबुद्धि से जो कार्य अनुष्ठित होता है, उसको तामस धर्म कहते हैं।
धर्म के भाग
धर्म के तीन भाग होते हैं।
दार्शनिक भाग – इसमें धर्म का सारा विषय अर्थात् मूल तत्त्व, उद्देश्य भाग और लाभ के उपाय निहित हैं।
पौराणिक भाग – यह स्थूल उदाहरणों के द्वारा दार्शनिक भाग को स्पष्ट करता है। इसमें मनुष्यों एवं अतिप्राकृतिक पुरुषों के जीवन के उपाख्यान आदि लिखे हैं। इसमें सूक्ष्म दार्शनिक तत्त्व मनुष्यों या अतिप्राकृतिक पुरुषों के जीवन के उदाहरणों द्वारा समझाये गये हैं।
आनुष्ठानिक भाग – यह धर्म का स्थूल भाग है। इसमें पूजा-पद्धति, आचार, अनुष्ठान, शारीरिक विविध अंग-विन्यास, पुष्प, धूप, धूनी प्रभृति नाना प्रकार की इन्द्रियग्राह्य वस्तुएँ हैं। इन सबको मिलाकर आनुष्ठानिक धर्म का संगठन होता है। सारे विख्यात धर्मों के ये तीन विभाग हैं।
धर्म के अंग
धर्म के 3 अंग हैं – यज्ञ, दान और तप ।
यज्ञ
यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं – कर्म यज्ञ, उपासना यज्ञ और ज्ञान यज्ञ ।
कर्म यज्ञ के 6 प्रकार हैं –
- नित्य कर्म – सामान्य दिनचर्या के तहत किए जाने वाले कार्य नित्य कर्म हैं।
- नैमितिक कर्म – किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य नैमितिक कर्म हैं।
- काम्य कर्म – धन, पुत्र आदि की कामना से जो शास्त्रानुसार कर्म किया जाना है उसे काम्य कर्म कहते हैं। इसमें दान यज्ञ आदि पुण्य कर्म किये जाते हैं।
- आध्यात्मिक कर्म – परोपकार की भावना से प्रेरित होकर जो कर्म किये जाते हैं, वे आध्यात्मिक कर्म के अन्तर्गत हैं। समाज सेवा, देश सेवा आदि कर्म आध्यात्मिक होते हैं।
- आधिदैविक कर्म – वास्तु कर्म आदि आधिदैविक कर्म कहलाते हैं। ब्राह्मण भोजन, अथिति सत्कार आदि कर्म आधिभौतिक कर्म माने जाते हैं।
वहीं गृहस्थाश्रम में पंच महायज्ञ करना बताया गया है।
पंच महायज्ञ हैं – देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ ।
- देव यज्ञ – देवताओं के निमित्त हवन करना देव यज्ञ है।
- ऋषि यज्ञ – ऋपियों ने शास्त्र लिखकर मानव जाति को ज्ञान प्रदान किया है। इसलिये वेदाध्ययन वेद-पाठ, गीता-पाठ या और धर्मग्रन्थ का नियमपूर्वक अध्ययन करना ऋषि यज्ञ है।
- पितृ यज्ञ – पितरेश्वरों के लिये तर्पण पितृयज्ञ है।
- भूत यज्ञ – प्रति दिन गौ को ग्रास देना भूत यज्ञ है।
- अतिथि यज्ञ – अथिति, अभ्यागत, साधु, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी आदि को सम्मानपूर्वक भोजन कराना अतिथि यज्ञ है।
दान
दान के 3 प्रकार हैं – अभय दान, विद्या दान और अर्थ दान।
- अभय दान – शरणागत की रक्षा करना अभय दान है।
- विद्या दान – जिसके पास जो विद्या या कला है, वह दूसरों को सिखाना विद्या दान है।
- अर्थ दान – धनादि पदार्थों का दान करना अर्थ दान है।
तप
तप 3 प्रकार का है – कायिक, वाचिक और मानसिक। गीता के सत्रहवें अध्याय में इसकी विवेचना की गई है।
- कायिक तप – देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शारीरिक अर्थात् कायिक तप कहते हैं। व्रत, उपवास भी कायिक तप के अन्तर्गत आते हैं।
- वाचिक तप – मन को उद्वेग न करने वाले सत्य, प्रिय और हितकारक सम्भाषण को तथा स्वाध्याय को वाचिक तप कहते हैं।
- मानसिक तप – मन को प्रसन्न रखना, सौम्यता, मौन अर्थात् मुनियों के समान वृत्ति रखना, मनोनिग्रह और शुद्ध भावना इनको मानसिक तप कहते हैं।
जिस मनुष्य में विद्या, तप, दानशीलता, गुण, धर्म – इनमें से कुछ भी नहीं, वह पशु के समान है। मानव शरीर में धर्म ही विशेष है। यदि मनुष्य धर्म को धारण करता है तो वह पशु भाव से मनुष्य भाव की तरफ उन्नतशील होता है।
यथार्थ में धर्म ही लोक उन्नति का प्रधान साधन है। तप, दान, यज्ञ आदि शुभ कर्म द्वारा मनुष्य सांसारिक लोक में यश, बल और तेज प्राप्त करता है। धर्म के द्वारा लोक में उन्नत अवस्था को प्राप्त होता हुआ मानव निष्काम भाव रहने से जीवन मुक्त हो सकता है।
संबंधित आलेख
धर्म क्या है?
धर्म का स्वरूप